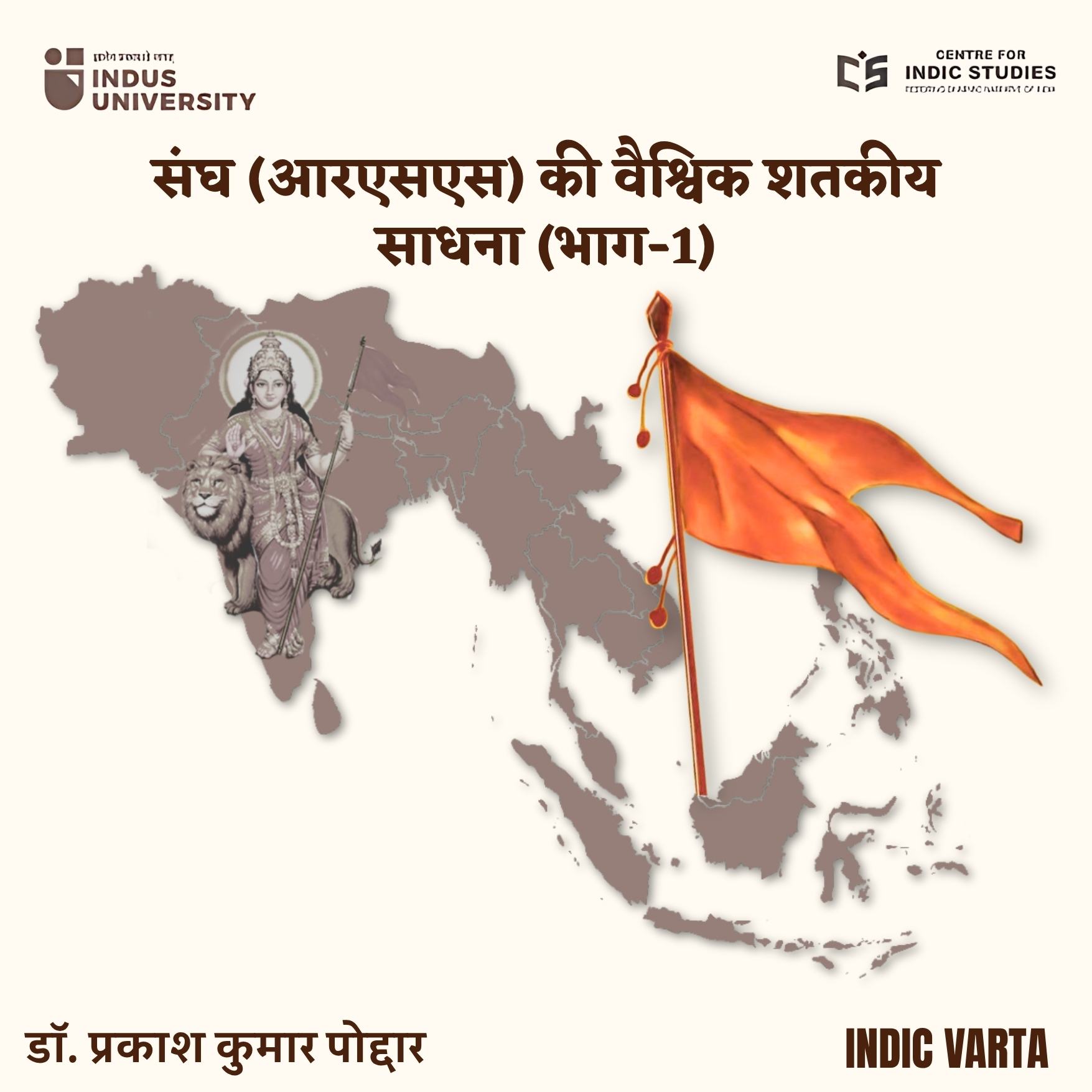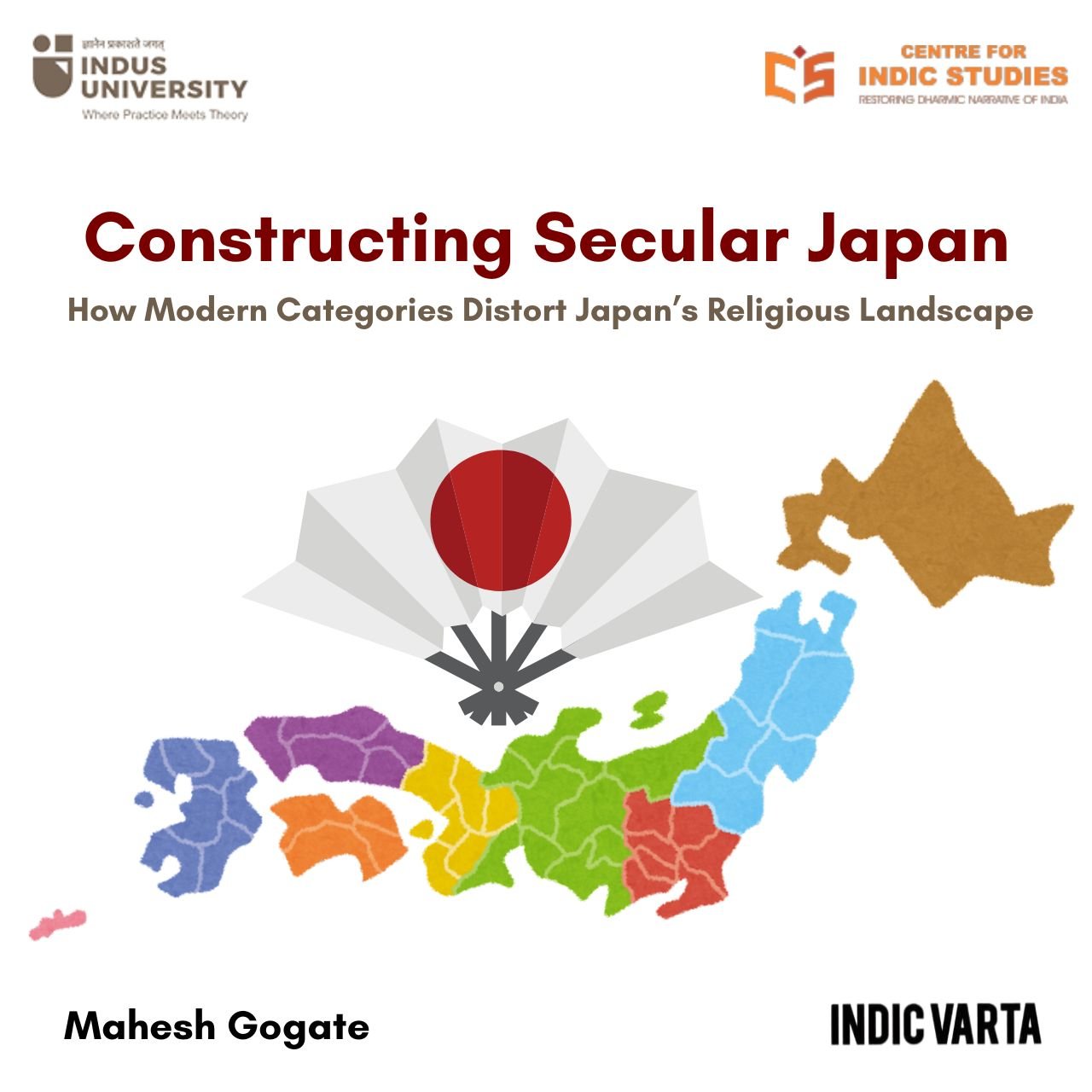डॉ. हेडगेवार ने भारतीय इतिहास को वर्तमान एवं भविष्य के धरातल पर भारत की राष्ट्रीयता के मूल प्रश्न पर विचार किया और संघ की स्थापना की। उनके अथक प्रयास से स्थापित राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अपने जन्म और अनौपचारिक विकास के कारण बीसवीं सदी में भारतीय इतिहास की अनोखी घटना मानी जाती है। इसके अस्तित्व में आने का उद्देश्य किसी सामाजिक व राजनीतिक विचारों की प्रतिक्रिया की जगह वास्तविक राष्ट्रवाद के साथ भारत की सदियों पुरानी परंपरा में निहित विचारों और कार्यों को अग्रेषित कर उसका निर्वहन है। दशकों से विदेशी शासकों द्वारा मानसिक, सांकृतिक और आर्थिक प्रताड़नाओं के फलस्वरूप आत्म-विस्मृत समाज को जागृत कर उसका समग्र उत्थान है। इसी उत्थान हेतु सर्वप्रथम व्यक्ति को राष्ट्र का प्रमुख क्रांतिकारी घटक मानते हुए उनके हृदय में राष्ट्र प्रेम की पवित्र भावना, सामूहिकता, सामाजिक संवेदनशीलता एवं एकता के भाव को संचारित करने का पहल किया गया। गुलामी की मानसिकता से अभिशप्त हिन्दू समाज का राष्ट्रीय पुनर्निर्माण हेतु व्यक्ति अथवा संघ की प्रतिबद्धता तभी कायम रह सकती है जब उसमें मातृभूमि के प्रति समर्पण, अनुशासन, संयम, साहस और वीरता आदि गुण समाहित हों। स्वयं के साथ दूसरों में भी इन गुणों का निर्माण कर उसे पोषित करना एक चुनौतीपूर्ण कार्य है। स्वामी विवेकानंद के अनुसार यह मानव-निर्माण का कार्य है। व्यक्ति और समाज में इन्हीं गुणों की अभिवृद्धि को ध्यान में रखते हुए संघ की संरचनात्मक व्यवस्था का निर्माण हुआ।
भारतीय परिदृश्य और संघ की स्थापना
यदि भारत के इतिहास पर दृष्टि डालें तो सोने की चिड़ियाँ कही जाने वाली भारत की ऐतिहासिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं आर्थिक पृष्ठभूमि गौरवमय रही है। कण-कण में व्याप्त सत्ता के अव्यक्त रूप का दर्शन करने वाला यह देश ‘वसुधैव कुटुंबकम्’ के भाव के साथ विश्व को आलोकित करता रहा है, परंतु भारत के इस स्वर्णिम गौरव का पिछले एक हजार वर्षों में बेतहाशा क्षरण हुआ। इस क्षरण की त्रासदी से मुक्ति का संघर्ष 19वीं सदी से लेकर 20वीं सदी के पूर्वार्द्ध तक अत्यंत गंभीर रहा है। हालांकि इससे पहले भी कई बड़े संघर्ष हुए, परंतु यह संघर्ष अंग्रेजों की गुलामी से मुक्ति का संघर्ष था। अनवरत गुलामी से मुक्ति हेतु बाह्य और आंतरिक संघर्ष की सर्वथा मुक्ति की कामना लिए डॉ. केशव बलिराम हेडगेवार ने विजया दशमी के पावन अवसर पर महाराष्ट्र के नागपुर में 27 सितंबर 1925 को ‘राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ’ की स्थापना की।
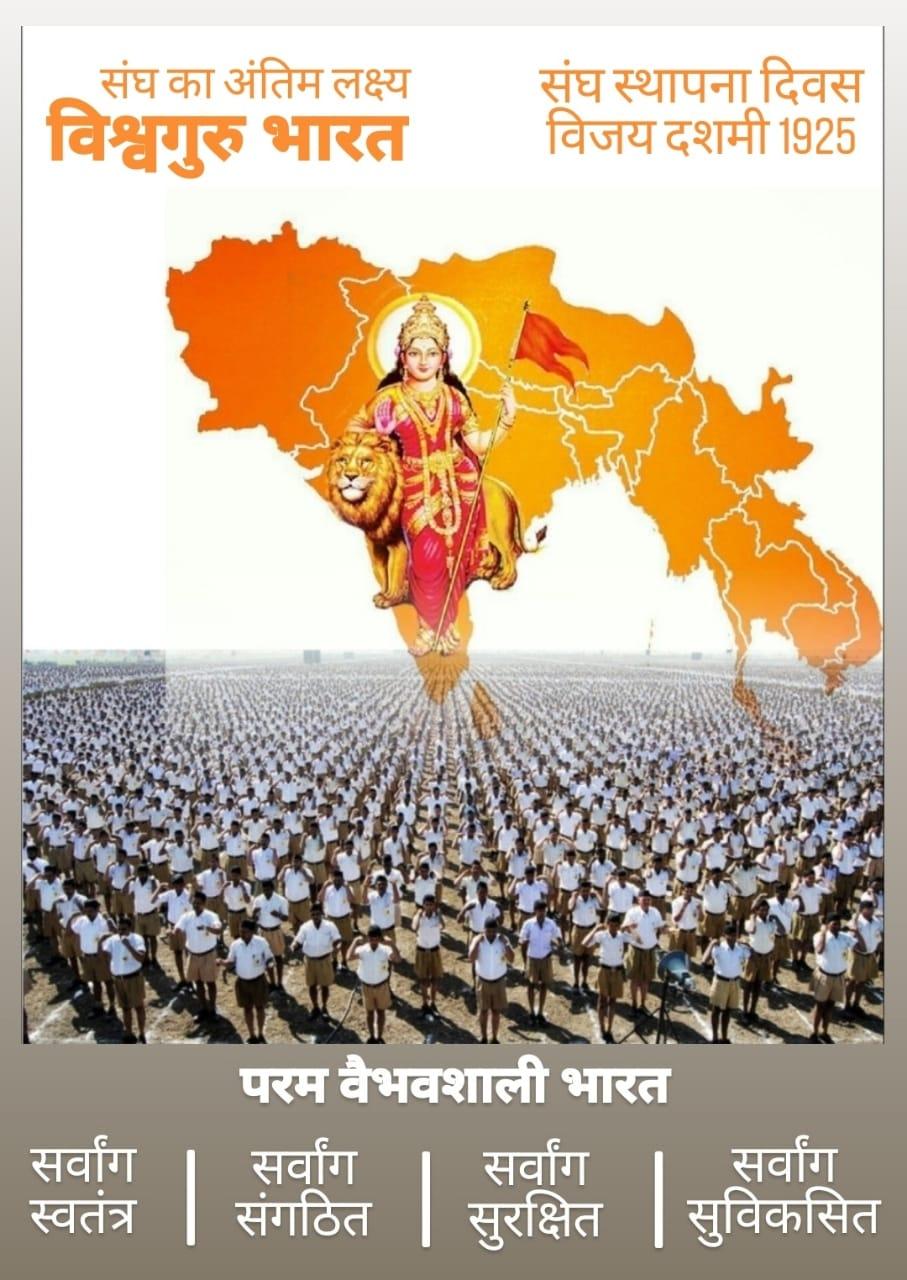
तत्कालीन परिस्थितियों में क्रांतिकारियों के समक्ष आजादी से मुक्ति के दो मार्ग थे, एक तो ‘क्रांति’ का जिससे तत्काल आजादी मिल सकती थी, दूसरा ‘व्यक्ति निर्माण से राष्ट्र निर्माण’ का। अर्थात, व्यक्ति के माध्यम से ऐसे समाज का निर्माण किया जाए जो आजादी तो प्राप्त करे ही साथ ही साथ वह अपने उन कमियों को भी दूर करे जिससे उनको पुनः दासता का सामना न करना पड़े। इसी क्रम में डॉ. हेडगेवार जी ने भारत की तत्कालीन परिस्थितियों का गहराई से अध्ययन किया और पाया कि जबतक उज्ज्वल चरित्रयुक्त समाज का निर्माण, देशवासियों में आत्मगौरव का भाव, समर्पण का भाव और संगठन शक्ति का विकास नहीं होगा तबतक वास्तविक रूप से आजादी नहीं हो सकती। क्योंकि इन गुणों के अभाव में एक शक्ति के जाने पर दूसरी शक्ति आकर हमें गुलाम बना लेगी जो पिछले शताब्दियों से होता आ रहा है।
क्रांतिबीज की उत्तरोत्तर वृद्धि हेतु साफ-सुथरी उर्वर भूमि वाला बाल मस्तिष्क की उपयुक्तता को ध्यान में रखते हुए डॉ. हेडगेवार ने संघ की शुरुआत बाल स्वयंसेवकों से की। रूढ़िगत समाज में स्थापित मान्यताओं के विरोध में जब कोई क्रांति के अंकुर फूटते हैं तो उसका समाज में उपहास, विरोध और फिर प्रशंसा अवश्य होती है। संघ संस्थापक डॉ. साहब को भी तत्कालीन सामाजिक उपेक्षाओं व उपहासों का सामना करना पड़ा। परंतु सामाजिक विसंगतियों से हृदय में जो व्यथा थी, वह द्रवित हो गंगा की आवेगयुक्त धारा की भांति किसी की परवाह किए बगैर पहाड़ों व खाइयों से गुजरती हुई शतकीय साधना में प्रवाहमान हो गई। अपनी दुरूह, संघर्षपूर्ण, दृढ़ संकल्पित यात्रा से संघ निरंतर सामाजिक एकता, सद्भाव, राष्ट्रभक्ति की भावना जाग्रत कर रही है। संघ की शतकीय साधना में केवल संगठनात्मक दस्तावेज शामिल नहीं है, बल्कि समर्पित महानुभावों के नेतृत्व में एक दार्शनिक यात्रा शामिल है। इस यात्रा में अभी तक जितने भी सरसंघचालक (संघ प्रमुख) हुए, वे सभी अपने-अपने जीवन के विविध अनुभवों के साथ विश्वविद्यालय की उच्च शैक्षणिक योग्यताओं से विभूषित थे।
संघ के संस्थापक डॉ. हेडगेवार स्वयं एक चिकित्सक थे। श्री गुरुजी प्राणिशास्त्र, राजनीतिशास्त्र एवं अंग्रेजी के विद्वान् थे। श्री बालासहेब देवरस कानूनविद् थे। श्री रज्जू भैया भौतिकी के प्रोफेसर थे। श्री के.एस. सुदर्शन एक दूरसंचार अभियंता थे और वर्तमान में श्री मोहनजी भागवत पशु चिकित्सक की उपाधि को प्राप्त हैं। संघ उत्तरोत्तर इन सरसंघचालकों के मार्गदर्शन में अपने दीर्घकालिक लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करते हुए निरंतर गतिमान है, चाहे वह अनुच्छेद-370 हो (जिसकी मांग संघ 1950 से करता आ रहा है), अयोध्या में राममंदिर का निर्माण हो आदि।
स्वयंसेवक की अवधारणा
डॉ. हेडगेवार जी का मानना था कि ‘लौकिक दृष्टि से समाज को समर्थ बनाने में हम तभी सफल हो सकेंगे जब उस प्राचीन परम्परा को युगानुकूल बना कर फिर से पुनरुज्जीवित कर पाएं। इस युग में जिस परिस्थिति में हम रहते हैं, ऐसे एक-एक, दो-दो, इधर-उधर बिखरे, पुनीत जीवन का आदर्श रखने वाले उत्पन्न होकर उनके द्वारा धर्म का ज्ञान, धर्म की प्रेरणा देने मात्र से काम नहीं होगा। आज के युग में तो राष्ट्र की रक्षा और पुन:स्थापना करने के लिए यह आवश्यक है कि धर्म के सभी प्रकार के सिद्धान्तों को अन्त:करण में सुव्यवस्थित ढंग से ग्रहण करते हुए अपना ऐहिक जीवन पुनीत बना कर चलने वाले और समाज को अपनी छत्र-छाया में लेकर चलने की क्षमता रखने वाले असंख्य लोगों का सुव्यवस्थित और सुदृढ़ जीवन एक सच्चरित्र, पुनीत, धर्मश्रद्धा से परिपूरित शक्ति के रूप में प्रकट हों और वह शक्ति समाज में सर्वव्यापी बनकर खड़ी हो। यह इस युग की आवश्यकता है। डॉ. हेडगेवार चाहते थे कि इस कार्य में सम्पूर्ण समाज लगे और समाज को इस काम के लिए प्रेरित, प्रशिक्षित करने का काम वह स्वयंस्फूर्त व्यक्ति करे जिसे स्वयंसेवक कहते हैं। 
इतना ही नहीं, बल्कि आज की सामाजिक परिस्थितियों में कुछ धार्मिक, निष्ठावान्, सत्यनिष्ठ साधक विद्वान् जो धर्म के सिद्धांतों को अपने अन्तःकरण में सुव्यवस्थित तरीके से ग्रहण कर ऐहिक जीवन को पुनीत बनाकर चलते हैं और समाज के असंख्य लोगों को अपने वात्सल्य की छाया में रखते हुए अपने जीवनानुभवों से उसे सींचते हैं। उन सभी के माध्यम से एक ऐसी राष्ट्र शक्ति का निर्माण हो जो सर्वव्यापी बनकर धर्मश्रद्धा से पूरित जागृत समाज के निर्माण में सहायक हो। इस शक्ति को पूर्ण करने में स्वयंस्फूर्त अहर्निश व्यक्ति ही स्वयंसेवक है। ऐसे स्वयंसेवकों के संगठन से भारत के गौरवमय विरासत के स्वर्णिम भविष्य का मार्ग प्रशस्त होगा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक इन्हीं बातों को ध्यान में रखकर निरंतर अपने ध्येय पथ पर गतिमान है।
हिन्दू बोध से तात्पर्य
डॉ. साहब ने बाल एवं किशोरों के साथ हिन्दू समाज को संगठित करने का कार्य प्रारंभ किया। यहाँ हिन्दू का अर्थ किसी पंथ, मजहब, उपासना पद्धति, रीलिजन आदि से नहीं है, बल्कि एक जीवन दृष्टि व पद्धति है। सर्वोच्च न्यायालय ने भी एक महत्त्वपूर्ण निर्णय में कहा है कि ‘हिन्दुत्व एक जीवन पद्धति’ है। सत्य एक है, उसे बुलाने के नाम अनेक हो सकते हैं, पाने के मार्ग भी अनेक हो सकते हैं, वे सभी समान हैं, यह मानना भारत की जीवन दृष्टि है और यही हिन्दू जीवन दृष्टि है। एक ही चैतन्य अनेक रूपों में अभिव्यक्त हुआ है। इसलिए सभी में एक ही चैतन्य विद्यमान है, विविधता में एकता यह भारत की जीवन दृष्टि है। इस जीवन दृष्टि को मानने वाला, भारत के इतिहास को अपना मानने वाला, यहाँ के जीवन मूल्यों को अपने आचरण से समाज में प्रतिष्ठित करने वाला और इनकी रक्षा हेतु त्याग और बलिदान करने वाले को अपना आदर्श मानने वाला हर व्यक्ति हिन्दू है, फिर उसका उपासना पन्थ चाहे जो हो। संघ का साफ मानना है कि भारत में रहने वाला इसाई या मुस्लिम बाहर से नहीं आया है। वे सब यहीं के हैं। हम सभी के पुरखे एक ही हैं, किसी कारण से मजहब बदलने से जीवन दृष्टि नहीं बदलती है। इसलिए उन सभी की जीवन दृष्टि भारत की याने हिन्दू ही है।


संघ की मौलिक साधना दृष्टि
इस संगठन के नामकरण को लेकर भी काफी चर्चाएँ की गई हैं। चर्चाओं में ‘शिवाजी संघ’, ‘जरीपटका मण्डल’, हिन्दू स्वयंसेवक संघ’ आदि नाम सुझाव के रूप में प्रस्तुत हुए, परंतु इन सभी नामों में सर्वसम्मति से 17 अप्रैल 1926 को ‘राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ’ निश्चित हुआ। 19 दिसम्बर 1926 में डॉ. हेडगेवार को ‘संघ प्रमुख’ के रूप में और उनके मार्गदर्शन में संघ के सुव्यवस्थित कार्य-संचालन के तहत उन्हें नवंबर 1926 में कार्यकर्ताओं द्वारा सरसंघचालक मनोनीत किया गया। डॉक्टर जी का मौलिक चिंतन सूक्ष्म और मूलग्राही था चाहे वह संघ की प्रार्थना को लेकर हो, उत्सव मनाने को लेकर हो या गुरु परंपरा के निर्वहन को लेकर। वे निर्विरोध गुरुस्थान में स्वयं को आरूढ़ कर प्रशंसित हो सकते थे, परंतु उन्होंने परम पवित्र भगवा ध्वज को ही गुरु मानकर संघ परंपरा में व्यक्तिनिष्ठता को निर्मूल कर दिया। मानव मन के अंदर से समाज में व्यभिचार उत्पन्न होने के जो महत्त्वपूर्ण साधन पद, पैसे आदि होते हैं उन सभी का सार्थक नियोजन संघ पद्धति में किया। यहाँ स्वयंसेवकों को पद के बजाय दायित्व और कर्तव्यों का निर्वाह करना होता है। कृतज्ञता और निरपेक्ष बुद्धि से संघ को अपना कार्य समझकर करने से तथा गुरु-दक्षिणा में अर्पित श्रद्धा सुमनों से न केवल धन की समस्या खत्म होती गई, बल्कि श्रद्धावान् कार्यकर्ताओं का निर्माण भी सहज होता चला गया। संघ जहां खड़ा हुआ, वहाँ से कार्य-विस्तार कैसे हो इस पर विचार करते हुए कार्यकर्ता अन्य प्रांतों में गए। वहाँ शिक्षा ग्रहण करने के साथ ही शाखाएँ शुरू की, कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण दिया। यह शिक्षण विभिन्न स्तरों के साथ संघ शिक्षा वर्ग के रूप में स्वयंसेवकों के लिए उत्तम रहा और संघ-कार्य का विस्तार होता गया।
किसी भी समाज में कुछ कमियाँ अवश्य होती हैं। हमारे भारतीय समाज में जातिवाद, संप्रदायवाद, क्षेत्रवाद, नस्लवाद, आतंकवाद आदि जैसे अनेक समस्याएँ रही हैं जिनका उन्मूलन कर समाज में सामाजिक समरसता लाने के लिए अनेक समजसेवियों ने अपना अथक प्रयास किया है। इस संबंध में संघ के दूसरे सरसंघचालक श्री माधवराव सदाशिवराव गोलवलकर जी ने कहा था कि, “समरसता के लिए आत्मग्लानि दूर करने के लिए आत्मबोध को जगाना पड़ेगा, स्वार्थ के स्थान पर निःस्वार्थ भाव का निर्माण करना पड़ेगा। सभी भेदों को भूलाकर, एकात्मकता का भाव जागृत कर एकरस, समरस, समाज का निर्माण करना पड़ेगा।” संघ इन्हीं बातों को ध्यान में रखकर अपना कार्य करता आ रहा है। इससे जो समविचारी संगठन जैसे स्वदेशी जागरण मंच, राष्ट्र सेविका समिति, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, वनवासी कल्याण आश्रम, विद्या भारती, विश्व हिन्दू परिषद, सेवा भारती, सामाजिक समरसता मंच, भारत विकास परिषद, आदि खड़े हुए, वे अपने-अपने महत्त्वपूर्ण उद्देश्यों के साथ सामाजिक समरसता की दिशा में कार्य कर रहे हैं। यही कारण है कि संघ की शाखाओं में स्वयंसेवकों के बीच जाति, वर्ग, क्षेत्र या भाषा के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं दिखाई देता है। वे सभी परिवार के सदस्य के रूप में होते हैं।

संघ के इसी स्वरूप को गांधीजी ने एक बार वर्धा (महाराष्ट्र) के संघ शिविर में देखा और पाया कि यहाँ सभी जातियों के लोग शिविर में भाग ले रहे हैं, जिनमें तथाकथित अस्पृश्य जातियों के स्वयंसेवक भी हैं और पारस्परिक रूप से सभी समानता एवं बंधुता के भाव के साथ शिविर में रह रहे हैं। इसे देखकर गांधी जी ने स्वयंसेवकों से कहा कि ‘आपके संगठन में अस्पृश्यता का अभाव देखकर मैं अत्यंत संतुष्ट हूँ।’ डॉ. भीमराव अंबेडकरजी का अनुभव भी ऐसा ही रहा है। डॉ. अंबेडकर ने 1939 में पुणे में आयोजित संघ शिविर को देखा तो उन्होंने कहा कि ‘यहाँ का सम्पूर्ण वातावरण अत्यंत पवित्र और समरस है। यहाँ पर सभी लोग अपने जातिगत पहचान को भूल गए हैं।’ उन्होंने माना कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखाओं में पारस्परिक समानता और सम्मान का जो भाव है वह सम्पूर्ण राष्ट्र में व्याप्त होना चाहिए। आज जो लोग राजनीतिक पृष्ठभूमि में सत्ता की स्वार्थ साधना करते हुए संघ के संबंध में दलित विरोधी और असहिष्णुता जैसे कुटिल और कुत्सित भ्रांतियाँ फैला रहे हैं उन्हें गांधी व अंबेडकर के विचारों पर अवश्य ध्यान देना चाहिए।
संघ स्वरूप और उसका युगानुकूल निर्वहन
संघ कार्य केवल संगठनात्मक काम-काज तक सीमित नहीं है, बल्कि एक गहन और कठिन साधना है। इसकी वैचारिकी सत्यनिष्ठ है। इसमें किसी का विरोध या द्वेष नहीं है। इस कार्य को समझना उनके लिए आसान हो जाता है जो श्रद्धा, भक्तिभाव और पवित्र मन से जिज्ञासा लेकर आता है और कठिन उनलोगों के लिए है जो किसी प्रकार का पूर्वाग्रह या उद्देश्य लेकर आता है। इसे सुनकर व पढ़कर समझना तो और भी कठिन है।
13 अक्टूबर 2024 में पांचजन्य के संपादकीय अंक में हितेश शंकर लिखते हैं ‘आरएसएस ने अपने स्थापना काल से ही भारतीय समाज को एकसूत्र में बांधने और उसकी आत्मशक्ति को जाग्रत करने का कार्य किया है। इसका उद्देश्य हमेशा से हिन्दू समाज को संगठित, सशक्त और संस्कारित करने का ही रहा है। भारत की सांस्कृतिक और सामाजिक धारा को अक्षुण्ण रखने तथा नई पीढ़ी को पुरखों-परंपराओं से जोड़े रखते हुए भविष्य के लिए तैयार करने का यह अप्रतिम कार्य संघ अपने स्थापना काल से करता आ रहा है।’
इसके साथ ही हमारे देश पर अनेक बाह्य आक्रमण व आंतरिक कलह से कई भाषा एवं संस्कृतियाँ प्रभावित हुईं। इन स्थितियों पर गंभीरता से विचार करने पर देखते हैं कि अनेक आपत्तियों-विपत्तियों के बीच अपने समाज के धर्मप्रधान जीवन के कुछ संस्कार अभी भी शेष बचे हैं। अर्थात, धर्म का पालन करने वाले, उसको अपने जीवन में अपनाने वाले तपस्वी, ज्ञानी, त्यागी एक अखंड परंपरा के रूप में उत्पन्न होते आए हैं। जिनकी वजह से न केवल हमारे राष्ट्र की रक्षा होती रही है, बल्कि उत्तरोत्तर विकास भी हुआ है। इन धरोहरों का रक्षण करते हुए समाज में उसका जागरण और अभ्यास से अभीष्ट परिवर्तन लाना भी संघ-कार्य में शामिल है।
आज के पाश्चात्य संस्कृति से अनुप्राणित समाज में यदि भारतीयता का गौरव जगाना है तो उस प्राचीन परंपरा को युगानुकूल बनाने होंगे। हमारे यहाँ की आध्यात्मिक सांस्कृतिक परंपरा युगानुकूल अलग-अलग स्वरूपों में खड़ी होती आई है। वह कभी गिरि-कन्दराओं में, जंगलों में रहने वाले तपस्वी के रूप में तो कभी योगी के रूप में। कभी यज्ञ-यागादि द्वारा तो कभी भगवद्भजन करने वाले भक्तों और संतों द्वारा यह परंपरा चली।
उन ज्ञान के विरासतों को समाज में प्रवाह हेतु संघ ने शाखा का आयोजन किया है। यह शाखा संघ का प्राण तत्त्व है। एक घंटे की नियमित शाखा में संस्कृत निष्ठ आज्ञाओं के साथ जो शारीरिक-बौद्धिक कार्यक्रम होते हैं उनका व्यक्तिगत जीवन में चारित्रिक गुणों के विकास के साथ सामाजिक उत्कर्ष छिपा होता है। क्योंकि यहाँ से जो स्वयंसेवक निकलते हैं वे व्यक्तिगत जीवन की आहुति चढ़ाने वाला, लोभ मोह आदि प्रलोभनों से दूर यहाँ तक कि स्वयं की कीर्ति का भी ध्यान नहीं रखता। वह एक ही ध्येय के साथ कि ‘तेरा वैभव अमर रहे माँ, हम दिन चार रहें न रहें’ पर आजीवन आरूढ़ रहता है। संघ विरोधियों ने शाखा की गतिविधियों को कॉपी करने का पुरजोर प्रयास किया, परंतु सफल नहीं हुए। क्योंकि उन्होंने उसकी शुरुआत ही ईर्ष्या, द्वेष व प्रतियोगी भावनाओं के साथ की।
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की एक घंटे की शाखा में ध्वजारोहण के पश्चात् द्रुतगतियोग, योग, आसन, सूर्य-नमस्कार, समता, दंड-प्रहार, निःयुद्ध, विभिन्न खेलों के बाद बैठक में देश प्रेम के गीत, प्रेरणास्पद कथा, कहानी, चर्चाएं, परिचय, सुभाषित, अमृतवचन और प्रार्थना में ‘भारत माता की जय’ के साथ ध्वजावतरण आदि प्रमुखता से शामिल है। इसमें आनेवाले स्वयंसेवकों में न केवल शारीरिक एवं बौद्धिक विकास होता है, बल्कि उज्ज्वल चरित्र का निर्माण भी शनैः शनैः हो जाता है। शाखा में प्रवेश हेतु उम्र की कोई सीमा निर्धारित नहीं है। अर्थात्, शिशु से लेकर प्रौढ़ और यहाँ तक कि वृद्ध व्यक्ति भी शामिल हो सकते हैं वह भी निःशुल्क।

इस शाखा में समाज के सभी लोग अपने-अपने व्यक्तिगत कार्यों से निवृत्त होकर सहजता से सम्मिलित हो सके इसके लिए शाखा लगाने का समय भी अलग-अलग है। जिसमें प्रभात शाखा, सायं शाखा, रात्रि शाखा, मिलन (सप्ताह में एक या दो बार लगने वाली शाखा), संघ मंडली (महीने में एक या दो बार लगने वाली शाखा)। इसके अलावा नियमित रूप से आयोजित की जाने वाली बैठकें, बौद्धिक वर्ग, घोष वर्ग के अंतर्गत घोष-वादन और उसका अभ्यास, संघ गीत, प्रार्थना, स्तोत्र, वर्ष भर में मनाए जाने वाले छः उत्सव (चैत्र शुक्ल पक्ष एकम को वर्ष प्रतिपदा, महाराज शिवाजी के जन्मदिन पर हिन्दू साम्राज्य दिनोत्सव, गुरु पूर्णिमा पर गुरु स्वरूप भगवा ध्वज पर श्रद्धा-सुमन अर्पण, आत्मीयता एवं बंधुत्व के रक्षण और विकास हेतु रक्षा बंधन, अधर्म पर धर्म की विजय की कामना हेतु विजयादशमी और मकर संक्रांति), शीत कालीन शिविर आदि। कार्यकर्ता प्रशिक्षण हेतु तीन दिनों का प्रारम्भिक वर्ग, सात दिनों का प्राथमिक वर्ग, पंद्रह दिनों का प्रथम संघ शिक्षा वर्ग, बीस दिनों का द्वितीय संघ शिक्षा वर्ग और पच्चीस दिनों का तृतीय संघ शिक्षा वर्ग के अलावा नगर से लेकर अखिल भारतीय स्तर तक के विभिन्न कार्यक्रम संघ की गतिविधियों में शामिल हैं।
इस प्रकार संघ आरंभिक दिनों से ही अपनी दिनचर्या में प्रमुखता से नियमित एक घंटे की शाखा साधना के साथ चरैवेति-चरैवेति अग्रसर है। इस क्रम में कई खरगोश की चाल के साथ उदित होकर संघ को रोकने, टोकने व प्रहार करने का प्रयास तो अवश्य किया, परंतु सत्य की राह पर संघर्ष करता हुआ संघ अविचल, अविरत धारा की भांति दृढ़ प्रतिज्ञ होकर विश्वव्यापी स्वरूप में परिणत होता गया। इस आलेख में हमने संघ के कुछ मौलिक व आधारभूत बातों को ही रखने का प्रयास किया है। आगामी आलेख में हम यह देखने का प्रयास करेंगे कि राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के उत्तरोत्तर शतकीय विकास में आसुरी प्रवृत्तियों से जो समय-समय पर घनघोर संकट के बादल छाए उसे विदीर्ण करने की साहस व क्षमता का परिचय संघ ने अपने सीमित साधनों व संसाधनों के माध्यम से किस प्रकार दिया।