- Visitor:200
- Published on: 2025-05-02 04:47 pm
भक्तकवि सूरदास का साहित्यिक एवं सामाजिक व्यक्तित्व
विलक्षण प्रतिभा के धनी सूरदास जी ने छः वर्ष की अवस्था में ही अपनी विद्या से सबको आश्चर्यचकित कर दिया था। वे किशोरावस्था में ही विरक्त होकर आगरा-मथुरा के बीच गऊघाट पर साधु के रूप में रहने लगे थे। चौरासी वैष्णवन की वार्ता के अनुसार गोवर्धन पर श्रीनाथ जी का मंदिर बन जाने के बाद जब बल्लभाचार्यजी गऊघाट पर आए तो सूरदास जी को उनके दर्शन हुए। सूरदास ने उन्हें अपना रचा हुआ एक पद सुनाया तो उन्होंने कहा “सूर ह्वैकै ऐसो घिघियात काहे को हौ, कछु भगवत्लीला वर्णन करौ।” इस संबंध में ब्रजेश्वर वर्मा लिखते हैं कि “तीन दिन तक गऊघाट पर रहकर महाप्रभु बल्लभ ने सूरदास और उनके सेवकों को श्रीमद्भागवत की अपनी सुबोधनी टीका का उपदेश दिया और पुरुषोत्तम सहस्त्रनाम सुनाया, जिससे सूरदास को सपूर्ण भागवत स्पष्ट हो गई और उसी के अनुसार पद रचने का उन्होंने संकल्प ले लिया।” सूरदास ने उनसे दीक्षा ली और इस प्रकार उस स्फुरित चेतना से उनमें भक्तिभाव की दिशा स्थिर होती गई। लोकज्ञान की विशदता एवं दिव्य-चक्षु सम्पन्न सूर ने अपने गुरु के आशीर्वाद और स्वाध्याय से सुमधुर स्वरों में कृष्ण-लीला का गान किया। उनका वही गान सूरसागर में संग्रहित है। सूरदास की भाषा ब्रजभाषा है और इसका हिन्दी से अभिन्न संबंध है। ध्यातव्य है कि मध्यकाल में हिन्दी क्षेत्र में राजस्थानी, मैथिली, खड़ीबोली, अवधी, ब्रज आदि भाषाओं का साहित्यिक भाषाओं के रूप में विकास हुआ है। हिन्दी की इन भाषाओं में सबसे अधिक लोकप्रिय भाषा ब्रजभाषा रही है जो अपनी कोमलता, लालित्य और मधुरता से हिन्दी क्षेत्र की प्रमुख काव्य-भाषा बनी रही। सूरदासजी ब्रजभाषा के प्रारम्भिक कवियों में से एक हैं। इसके बावजूद इनकी कविता की भाषा अत्यंत ही प्रौढ़, विकसित और समृद्ध है जो अपने वैभव एवं गांभीर्य से सभी को चकित कर देती है।
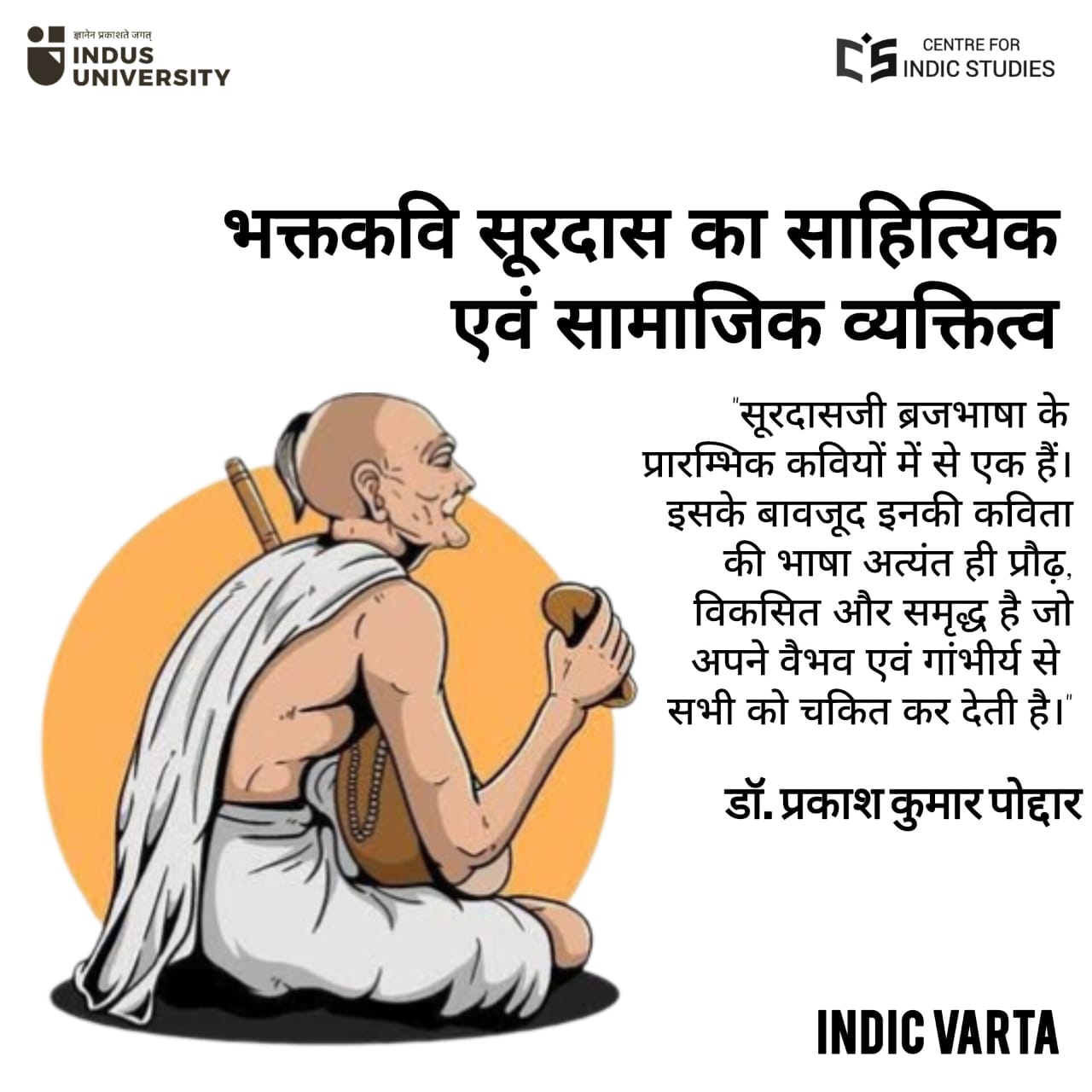
हिन्दुस्थान के हिन्दी साहित्य में सूर्य के समान चमकने वाले ब्रजभाषा के श्रेष्ठतम महाकवि सूरदास शुद्धाद्वैतवाद के प्रवर्तक और पुष्टिमार्ग के संस्थापक श्रीबल्लभाचार्य के अनन्य शिष्य और भगवान् श्रीकृष्ण के परम भक्त थे। हिन्दी साहित्य में इनका संबंध भक्तिकाल के सगुण धारा में कृष्ण-भक्ति शाखा से है। इन्होंने अपने महाकाव्य सूरसागर में श्रीकृष्ण की बाल-लीला तथा भ्रमरगीत के अंतर्गत गोपिकाओं के साथ शृंगार-वर्णन का अत्यंत ही सटीक, जीवंत और अप्रतिम वर्णन किया है। इसलिए हिन्दी के कवियों की जब बात आती है तो महाकवि सूरदास की सूरता अपनी संपूर्णता के साथ दैदीप्यमान हो जाता है। उनके संदर्भ में एक लोक-प्रचलित पद स्मरणीय है:
“सूर-सूर तुलसी ससि उडगन केशवदास।।
और कवि खाड्योतसम जहँ-तहँ करत प्रकास।।”
डॉ. राजेश श्रीवास्तव अपने हिन्दी साहित्य के प्राचीन इतिहास में लिखते हैं कि “कृष्ण भक्ति की अजस्र धारा को प्रवाहित करने वाले भक्त कवियों में सूरदास का नाम सर्वोपरि है। हिन्दी साहित्य में भगवान् श्रीकृष्ण के अनन्य उपासक और ब्रजभाषा के श्रेष्ठ कवि महात्मा सूरदास हिन्दी साहित्य के सूर माने जाते हैं।”
हिन्दू पंचांग के अनुसार महाकवि सूरदास का प्राकट्य दिवस बैशाख मास के शुक्ल पक्ष के पंचमी तिथि को माना जाता है। वे जन्मांध, परंतु आंतरिक दिव्य दृष्टि से सम्पन्न कवि थे। उनके जन्म को लेकर विद्वानों में मतभेद है। कुछ इतिहासकार उनका समय 1478-1581 ई. के बीच हरियाणा के फरीदाबाद में स्थित सीही ग्राम में मानते हैं तो कुछ आगरा के पास रुनकता में मानते हैं। इनका निवास स्थान गऊघाट, वृंदावन एवं पारसोली माना जाता है।
विलक्षण प्रतिभा के धनी सूरदास जी ने छः वर्ष की अवस्था में ही अपनी विद्या से सबको आश्चर्यचकित कर दिया था। वे किशोरावस्था में ही विरक्त होकर आगरा-मथुरा के बीच गऊघाट पर साधु के रूप में रहने लगे थे। चौरासी वैष्णवन की वार्ता के अनुसार गोवर्धन पर श्रीनाथ जी का मंदिर बन जाने के बाद जब बल्लभाचार्यजी गऊघाट पर आए तो सूरदास जी को उनके दर्शन हुए। सूरदास ने उन्हें अपना रचा हुआ एक पद सुनाया तो उन्होंने कहा “सूर ह्वैकै ऐसो घिघियात काहे को हौ, कछु भगवत्लीला वर्णन करौ।” इस संबंध में ब्रजेश्वर वर्मा लिखते हैं कि “तीन दिन तक गऊघाट पर रहकर महाप्रभु बल्लभ ने सूरदास और उनके सेवकों को श्रीमद्भागवत की अपनी सुबोधनी टीका का उपदेश दिया और पुरुषोत्तम सहस्त्रनाम सुनाया, जिससे सूरदास को सपूर्ण भागवत स्पष्ट हो गई और उसी के अनुसार पद रचने का उन्होंने संकल्प ले लिया।” सूरदास ने उनसे दीक्षा ली और इस प्रकार उस स्फुरित चेतना से उनमें भक्तिभाव की दिशा स्थिर होती गई। लोकज्ञान की विशदता एवं दिव्य-चक्षु सम्पन्न सूर ने अपने गुरु के आशीर्वाद और स्वाध्याय से सुमधुर स्वरों में कृष्ण-लीला का गान किया। उनका वही गान सूरसागर में संग्रहित है।
सूरदास की प्रमुख कृतियों में सूरसागर, साहित्यलहरी, सूरसारावली, राधारसकेलि, आदि हैं। सूरसागर विश्वप्रसिद्ध रचना है जो गेय पदों का विशाल संग्रह माना जाता है। इसकी रचना पद्धति श्रीमद्भागवत के अनुरूप द्वादश स्कंधों में हुई है। इसमें सबसे मर्मस्पर्शी अंश भ्रमरगीत प्रसंग है जिसमें गोपियों की वाक्विदग्धता अत्यंत मनोहारिणी है। ऐसा माना जाता है कि सूरसागर में पदों की संख्या सवा लाख थी जिसमें गोपियों की वाक्पटुता में से अब केवल दस हजार ही मिलते हैं। सूरसारावली विवादित होने के बावजूद प्रामाणिक है। इसमें छंदों की संख्या 1107 है। साहित्य लहरी में नायिका भेद और अलंकार निरूपण है जो दृष्टकूट पद है और रीतिशस्त्र से सम्बद्ध है। इसमें पदों की संख्या 118 है।
सूरदास की भाषा ब्रजभाषा है और इसका हिन्दी से अभिन्न संबंध है। ध्यातव्य है कि मध्यकाल में हिन्दी क्षेत्र में राजस्थानी, मैथिली, खड़ीबोली, अवधी, ब्रज आदि भाषाओं का साहित्यिक भाषाओं के रूप में विकास हुआ है। हिन्दी की इन भाषाओं में सबसे अधिक लोकप्रिय भाषा ब्रजभाषा रही है जो अपनी कोमलता, लालित्य और मधुरता से हिन्दी क्षेत्र की प्रमुख काव्य-भाषा बनी रही। सूरदासजी ब्रजभाषा के प्रारम्भिक कवियों में से एक हैं। इसके बावजूद इनकी कविता की भाषा अत्यंत ही प्रौढ़, विकसित और समृद्ध है जो अपने वैभव एवं गांभीर्य से सभी को चकित कर देती है।
महाकवि सूरदास के काव्यों में भक्ति, शृंगार, और वात्सल्य का अद्भुत मिश्रण है। सूरसागर और सूरसारावली में राधा और कृष्ण के प्रेम का अद्भुत चित्रण है। सगुण-भक्ति काव्य-धारा में श्रीकृष्ण के अनन्य उपासक सूरदास जी के कुछ काव्य-पक्तियों का दृश्यावलोकन करने का लघु प्रयास उनकी जयंती के शुभ अवसर पर यहाँ किया जा रहा है।
भक्तिपरक काव्य
सूरदास की भक्ति सख्य-भाव की है। चौरासी वैष्णवन की वार्ता (हिन्दी का एक ऐतिहासिक ग्रंथ) के उद्धरणों से स्पष्ट होता है कि अष्टछाप के सभी कवि ध्रुपद शैली के गायक थे। अष्टछाप के सर्वश्रेष्ट कवियों में कवि सूरदास में भक्ति भावना का उत्कर्ष उनके काव्य की आत्मा थी। उनके भक्ति का मेरुदंड पुष्टिमार्ग है, जिसमें भगवान का अनुग्रह ही भक्त का कल्याण करके उसे इस संसार सागर से पार लगाने में सहायक है। वे कहते हैं:
“जापर दीनानाथ ढरै।
सोइ कुलीन बड़ौ सुन्दर सोइ, जा पर कृ पा करै।
सूर पतित तरि जाय तनक में, जो प्रभु नेक ढरै॥”
महात्मा सूरदास ने अपना सर्वस्व कृष्ण के चरणों में अर्पित कर पुष्टिमार्ग को अपनाया था। इस भक्ति-भावना में दैन्य भाव की प्रधानता है, जिसमें व्यक्ति अपने अहम का परित्याग कर देता है। भक्त यह मानता है कि उनकी दीनता से द्रवित होकर ईश्वर अपनी शरण में ले लेगा। भक्ति के उद्गार कुछ इस प्रकार हैं:
“मोसों पतित न और गोसाईं।
अवगुण मोपै अजहुँ न् छुटत बहुत पच्चों अब ताईं।
सूर पतित कौं ठौर कहूँ नहिं राखि लेहु सरनाई।।”
सूरदास परब्रह्म के रूप में योगेश्वर श्रीकृष्ण के सगुण का मंडन तथा निर्गुण का खंडन करते हैं। उन्होंने प्रेम से वशीभूत होकर अवतार लिया है। इस संदर्भ में वे गोपियों से कहलवाते हैं:
“निरगुन कौन देश को बासी।
को है जनक को है जननी ।
कौन नारी को दासी ।।”
उनके पदों में भक्ति की अन्ययता अप्रतिम है।
“मेरो मन अनत कहाँ सुख पावै।
जैसे उड़ि जहाज को पंछि, पुनि जहाज पर आवै।।”
शृंगार वर्णन
माधुर्य भाव में सूरदास ने संयोग और वियोग दोनों का मार्मिक चित्रण किया है। बालक कृष्ण राधा को देखते ही उनपर आकर्षित होते हैं:
“बूझत श्याम कौन तू गोरी।
कहाँ रहति काकी तू बेटी, देखी नहीं कबहूँ ब्रजखोरी।।”
बाल कृष्ण गाय को दुहते समय एक धार दूध के पात्र में तो दूसरे धार को राधा की ओर डालते हैं तो उसका चित्रण सूरदास जी इस प्रकार करते हैं:
“धेनु दुहत अति ही रति बाढ़ी।
एक धार दोहनी पहुंचावति, एक धार जहँ प्यारी ठाढी।।”
वियोग शृंगार का चित्रण भी काफी मार्मिक है। कृष्ण में रत गोपियों को जो लताऐं शीतलता प्रदान कर रही थीं वही अब बिछुड़ने पर आग की ज्वाला बन गई है। अर्थात, अत्यंत दुखदायी हो गई है:
“बिनु गोपाल बैरिन भईं कुंजै।
तब वै लता लगति तन शीतल,
अब भईं विषम ज्वाल की पुंजै।।”
हिन्दी के मूर्धन्य साहित्यकार आचार्य रामचन्द्र शुक्ल लिखते हैं कि “कृष्ण के मथुरा चले जाने पर गोपियों का जो विरह सागर उमड़ा है उसमें मग्न होने पर तो पाठकों को कहीं ठहराव ही नहीं मिलता। वियोग की जितनी भी दशाएं हो सकती हैं सबका समावेश उसके भीतर है।” उन्होंने आगे कहा कि शृंगार का रस-राजत्व यदि किसी ने दिखाया है तो वह सूरदास ने दिखाया है।
वात्सल्य वर्णन
सूरदास वात्सल्य के सम्राट कहे जाते हैं। वे बाल मनोभावों के चित्रण के कुशल चितेरे हैं। पुरुष होते हुए भी उनमें माँ का कोमल हृदय है। माँ यशोदा पालने में श्रीकृष्ण को झूला रही हैं:
“यशोदा हरि पालने झुलावै।
हलरावै, दुलरावै, मल्हावै, जोई सोई कछु गावै।
मेरे लाल को आऊ निदरिया कहे न बेगि आवै।।”
कृष्ण के बाल रूप का वर्णन बहुत ही सुंदर ढंग से सूर ने किया है:
“किलकत कान्ह घुटरुवन आवत।
मनिमय कनक नन्द के आँगन, बिम्ब पकरिबे धावत।।”
कृष्ण जी अपने मुख पर दधि का लेप कर परछाईं को पकड़ने के लिए दौर रहे हैं, सूरदास जी कहते हैं:
“सोभित कर नवनीत लिए।
घुटरुवन चलत रेनु-तन मंडित, मुख दधि लेप किए।।”
बालक की चपलता और अपने चोरी को छुपने की तार्किकता का मनोरम चित्रण इस प्रकार है:
“मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो।
ग्वाल बाल सब बैर परत हैं, बरबस मुख लपटायो।।”
वात्सल्य में संयोग के साथ वियोग का चित्रण भी अत्यंत मार्मिक है। यशोदा को यह विश्वास है कि जितना अधिक ख्याल वो कृष्ण को रख सकती हैं उतना उसकी सगी माँ देवकी भी नहीं:
“संदेशों देवकी सों कहियो।
हौं तो धाय तिहारे सुत की, दया करत ही रह्यो।”
सूरदास के वात्सल्य वर्णन में सहजता, मनोवैज्ञानिकता, स्वाभाविकता, तन्मयता, सरलता आदि गुणों के कारण हृदय को आकृष्ट करने की पूर्ण क्षमता विद्यमान है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं “यशोदा के बहाने सूरदास ने मातृहृदय का ऐसा स्वाभाविक सरल और हृदयग्राही चित्र खींचा है कि आश्चर्य होता है।”
निष्कर्ष
इस प्रकार हम देखते हैं कि सूरदास के काव्य में चित्रात्मकता, बिम्बात्मकता, कोमलता, भावगर्भिता, बोधकता, संक्षिप्तता आदि गुणों के दर्शन से यह अपने काव्य-सौन्दर्य की दृष्टि से सर्वकालिक आदर्श में स्वभावतः प्रतिष्ठित हो जाते हैं। सूर की काव्य प्रतिभा के संदर्भ में हिन्दी के प्रसिद्ध विद्वान आचार्य हर्जारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं “सूरदास जब अपने प्रिय विषय का वर्णन शुरू करते हैं तो मानो अलंकार शास्त्र हाथ जोड़कर उनके पीछे-पीछे दौड़ा करता है। उपमाओं की बाढ़ आ जाती है, रूपकों की वर्षा होने लगती है। संगीत के प्रवाह में कवि स्वयं बह जाता है। वह अपने को भूल जाता है। काव्य में इस तन्मयता के साथ शास्त्रीय पद्धति का निर्वाह विरल है।”
इसके अलावा इनके काव्य का भाव पक्ष भी तत्कालीन समाज का मार्गदर्शन करती है। इन्होंने अपने काव्य में सामाजिक उत्पीड़न, विदेशी आक्रमण, सांस्कृतिक पराभव और मानमर्दन, निर्धनता, अशिक्षा, रोग, शोक आदि के कारण आयी मानसिक कटुता, उद्वेष और निराशा को धोकर समाज में नई जीवन-स्फूर्ति का संचार किया। तत्कालीन समाज में लोकमानस के मानसिक अवरोध को दूर किया और एक कुंठामुक्त समाज को जीवन-निर्वाह के योग्य बना दिया।
सबसे ध्यान देने योग्य बात है कि हिन्दी साहित्य का भक्तिकाल भक्ति-आंदोलन से अनुस्यूत है। जिसमें भारत के एकीकरण में भक्ति की अनिवार्य भूमिका मानी जाती है वह भी तब जब मुगलों द्वारा खून-खराबे, धर्मांतरण एवं हमारे हिन्दू मंदिरों को तोड़ा जा रहा हो। ऐसी विषम परिस्थितियों में भारत के चारों ओर से भक्ति की जो लहर उठी उसने हिन्दू चेतना को मुखरता प्रदान की। भारत एक बार पुनः अपनी धार्मिक-सांस्कृतिक चेतना के साथ जीवंत हो उठा। इस जीवंतता को समृद्ध करने में भक्ति की निर्गुण धारा के साथ सगुण धारा के रूप में राम एवं कृष्ण की भक्ति की अनुगूँज ने समस्त भारतीयों में नवरस का संचार किया और एक बार पुनः समस्त भारत भक्ति रस से भावविभोर होकर एकमेव हो गया। इस रस के संचार में सुर, तुलसी, कबीर आदि भक्त कवियों ने अहम भूमिका निभाई।
- 100 min read
- 4
- 0










