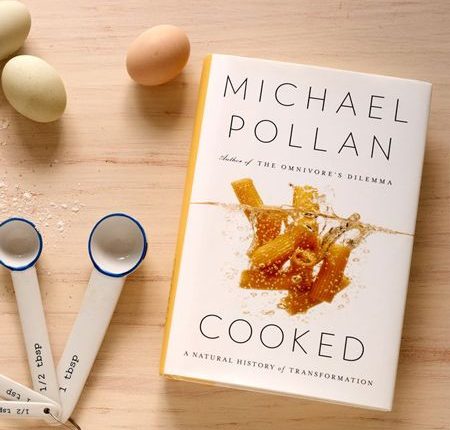- Visitor:336
- Published on: 2024-11-25 11:31 am
पद्म पुराण में वर्णित आश्रम व्यवस्था का संक्षिप्त स्वरूप
मनुष्य के व्यवस्थित जीवन-प्रणाली की सार्थक व्यवस्था हमारे सनातन धर्म में ‘आश्रम व्यवस्था’ के रूप में रूपायित है जिसका अवलोकन हम यहाँ करने जा रहे हैं।

हिंदू धर्म में व्यक्ति के जीवन को चार मुख्य चरणों (आश्रमों) में विभाजित किया गया है। यह चरण जीवन के विभिन्न अवस्थाओं पर आधारित है और व्यक्ति के धार्मिक, सामाजिक और आध्यात्मिक कर्तव्यों का निर्धारण करती है। ये चार चरण (आश्रम) इस प्रकार हैं: (क) ब्रह्मचर्य आश्रम (शिक्षा और अनुशासन): यह जीवन का पहला चरण है। जब व्यक्ति विद्यार्थी होता है और गुरु से शिक्षा प्राप्त करता है। इस दौरान वह ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए ज्ञान की प्राप्ति के लिए समर्पित होता है; (ख)गृहस्थ आश्रम (पारिवारिक जीवन): यह दूसरा चरण है। जब व्यक्ति विवाह करता है और परिवार का भरण-पोषण के साथ समाज सेवा और धार्मिक कर्तव्यों का पालन करता है; (ग) वानप्रस्थ आश्रम (संन्यास की तैयारी): यह जीवन का तीसरा चरण है। इसमें व्यक्ति परिवार की जिम्मेदारियों से मुक्त होकर साधारण जीवन व्यतीत करता है। इस दौरान वह आध्यात्मिक साधना के माध्यम से आत्म-ज्ञान की खोज करता है; एवं (घ) संन्यास आश्रम (मोक्ष की ओर): यह अंतिम चरण है। इसमें व्यक्ति मोक्ष प्राप्ति के लिए तपस्या, ध्यान और आध्यात्मिक साधना करता है। इसका उद्देश्य आत्मा की मुक्ति और परमात्मा से एकाकार होना है।
जीवन की विभिन्न अवस्थाओं में अपनाए जाने वाले जो उपर्युक्त आश्रम व्यवस्था निर्धारित किया गया है उसका विस्तार से वर्णन पद्म पुराण (संक्षिप्त), गीत प्रेस, गोरखपुर, पृष्ठ 60-63) में है। यहाँ उन्हीं वर्णनों को हम जानने का प्रयास करेंगे जिसे आत्मसात कर जीवन को उन्नत बनाया जा सके।
ब्रह्मचर्य आश्रम व्यवस्था
धर्म और अर्थ के तत्त्व की जिज्ञासा वाले पुरुष को चाहिए कि वह अपनी आयु के एक चौथाई भाग तक दूसरे की निंदा से बचकर ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए गुरु अथवा गुरुपुत्र के समीप निवास करे तथा गुरु की पूजा से जो समय बचे, उसमें अध्ययन करे, श्रद्धा और आदर-पूर्वक गुरु का आश्रय ले। गुरु के घर में रहते समय गुरु के सोने के पश्चात् शयन करे और उनके उठने से पहले उठ जाए। वह सदा गुरु का किंकर होकर सब प्रकार की सेवाएं करे। सब कार्यों में कुशल हो। पवित्र, कार्यदक्ष और गुणवान् बने। गुरु को प्रिय लगने वाला उत्तर दे। इंद्रियों को जीतकर शांत भाव से गुरु की ओर देखे। गुरु के भोजन करने से पहले भोजन और जलपान करने से पहले जलपान न करे। गुरु खड़े हों तो स्वयं बैठे नहीं। उनके सोये बिना शयन भी न करे। उत्तान हाथों के द्वारा गुरु के चरणों का स्पर्श करे। गुरु के दाहिने पैर को अपने दाहिने हाथ से और बाएं पैर को अपने बाएं हाथ से धीरे-धीरे दबाए और इस प्रकार प्रणाम करके गुरु से कहे –
‘भगवन् ! मुझे पढ़ाइए। प्रभो ! यह कार्य मैंने पूरा कर लिया है और इस कार्य को मैं अभी करूंगा।’
इस प्रकार पहले कार्य करे और फिर किया हुआ सारा काम गुरु को बाता दे। वह एक, दो, तीन या चारों वेदों को अर्थ सहित गुरुमुख से अध्ययन करे। भिक्षा के अन्न से जीविका चलाये और धरती पर शयन करे। वेदोक्त व्रतों का पालन करता रहे और गुरु दक्षिणा देकर विधिपूर्वक अपना समावर्तन-संस्कार करे। फिर धर्मपूर्वक प्राप्त हुई स्त्री के साथ गार्हपत्यादि अग्नियों की स्थापना करके प्रतिदिन हवनादि के द्वारा उनका पूजन करे।
गृहस्थ आश्रम व्यवस्था
आयु का प्रथम भाग ब्रह्मचर्याश्रम में बीताने के पश्चात् गृहस्थ आश्रम में व्यतीत करे। गृहस्थ ब्राह्मण यज्ञ करना, यज्ञ कराना, वेद पढ़ना, वेद पढ़ाना तथा दान देना और दान लेना – इन छः कर्मों का अनुष्ठान करे। गृहस्थ के व्रत से बढ़कर दूसरा कोई महान् तीर्थ नहीं बताया गया है। गृहस्थ पुरुष कभी केवल अपने खाने के लिए भोजन न बनाये, बल्कि देवता और अतिथियों के उद्देश्य से ही रसोई करे। पशुओं की हिंसा न करे। दिन में कभी नींद न ले। रात के पहले और पिछले भाग में भी न सोये। सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय भोजन न करे। झूठ न बोले। गृहस्थ के घर में कभी ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई ब्राह्मण अतिथि आकर भूखा रह जाय और उसका यथावत् सत्कार न हो। अतिथियों को भोजन कराने से देवता और पितर संतुष्ट होते हैं; अतः गृहस्थ पुरुष सदा ही अतिथियों का सत्कार करे। जो वेद-विद्या और व्रत में निष्णात, श्रोत्रिय, वेदों के पारगामी, अपने कर्म से जीविका चलाने वाले, जितेंद्रिय, क्रियावान् और तपस्वी है, उन्हीं श्रेष्ठ पुरुषों के सत्कार के लिए हव्य और कव्य का विधान किया गया है। जो नश्वर पदार्थों के प्रति आसक्त है, अपने कर्म से भ्रष्ट हो गया है, अग्निहोत्र छोड़ चुका है, गुरु की झूठी निंदा करता है और असत्य भाषण में आग्रह रखता है, वह देवताओं और पितरों को अर्पण करने योग्य अन्न के पाने का अधिकारी नहीं है। गृहस्थ की संपत्ति में सभी प्राणियों का भाग होता है। जो भोजन नहीं बनाते, उन्हें भी गृहस्थ पुरुष अन्न दे। वह प्रतिदिन ‘विघस’ और ‘अमृत’ भोजन करे। यज्ञ से (देवताओं और पितर आदि को अर्पण करने से) बचा हुआ अन्न हविष्य के समान एवं अमृत माना गया है। तथा जो कुटुंब के सभी मनुष्यों के भोजन कर लेने के पश्चात् उनसे बचा हुआ अन्न ग्रहण करता है; उसे ‘विघसाशी’ (‘विघस’ अन्न का भोजन करने वाला) कहा गया है।
गृहस्थ पुरुष को केवल अपनी ही स्त्री से अनुराग रखना चाहिए। वह मन को अपने वश में रखे, किसी के गुणों में दोष न देखे और अपनी सम्पूर्ण इंद्रियों को काबू में रखे। ऋत्विक, पुरोहित, आचार्य, मामा, अतिथि, शरणागत, वृद्ध, बालक, रोगी, वैद्य, कुटुंबी, संबंधी, बांधव, माता, पिता, दामाद, भाई, पुत्र, स्त्री, बेटी तथा दास-दासियों के साथ विवाद नहीं करना चाहिए। जो इनसे विवाद नहीं करता, वह सब प्रकार के पापों से मुक्त हो जाता है। जो अनुकूल वर्ताव के द्वारा इन्हें अपने वश में कर लेता है, वह सम्पूर्ण लोकों पर विजय पा जाता है – इसमें तनिक भी संदेह नहीं है।
गृहस्थ ब्राह्मण की तीन जीविकाएं हैं। पहली है – कुम्भधान्य वृत्ति, जिसमें एक गहरे से अधिक धान्य का संग्रह न करके जीवन-निर्वाह किया जाता है। दूसरी उंछशिल वृत्ति है, जिसमें खेती कट जाने पर खेतों में गिरी हुई अनाज की बालें चुनकर लायी जाती है और उन्हीं से जीवन निर्वाह किया जाता है। तीसरी कापोती वृत्ति है, जिसमें बाजार और खलिहान से अन्न के बिखरे हुए दाने चुनकर लाए जाते हैं तथा उन्हीं से जीविका चलायी जाती है। जहां इन तीन वृत्तियों से जीविका चलाने वाले पूजनीय ब्राह्मण निवास करते हैं, उस राष्ट्र की वृद्धि होती है। जो ब्राह्मण गृहस्थ की इन तीन वृत्तियों से जीवन निर्वाह करता है और मन में कष्ट का अनुभव नहीं करता, वह दस पीढ़ी तक के पूर्वजों को तथा आगे होने वाली संतानों की दस पीढ़ियों को पवित्र कर देता है।
वानप्रस्थ आश्रम व्यवस्था
प्रत्येक द्विज को अपनी आयु का तीसरा भाग वानप्रस्थ आश्रम में रहकर व्यतीत करना चाहिये। गृहस्थ पुरुष जब यह देख ले कि मेरे शरीर में झुर्रियां पड़ गयी हैं, सिर के बाल सफेद हो गए हैं और पुत्र के भी पुत्र हो गए हैं, तब वह वन में चला जाय।
वहाँ वह अग्नियों का सेवन करे, देवताओं का पूजन करे, नियम पूर्वक रहे, नियमित भोजन करे, भगवान् श्रीविष्णु में भक्ति रखे तथा यज्ञ के सम्पूर्ण अंगों का पालन करते हुए प्रतिदिन अग्निहोत्र का अनुष्ठान करे। धान और जौ वही ग्रहण करे, जो बिना जोती हुई जमीन में अपने-आप पैदा हुआ हो। इसके सिवा नीवार (तीना) और विघस अन्न को भी वह पा सकता है। उसे अग्नि में देवताओं के निमित्त हविष्य भी अर्पण करना चाहिये।
वानप्रस्थी लोग वर्षा के समय खुले मैदान में आकाश के नीचे बैठते हैं, हेमन्त ऋतु में जल का आश्रय लेते हैं और ग्रीष्म में पंचाग्नि-सेवनरूप तपस्या करते हैं। उनमें से कोई तो धरतीपर लोटते हैं, कोई पंजों के बल खड़े रहते हैं और कोई-कोई एक स्थानपर एक आसन से बैठे रह जाते हैं। कोई दाँतों से ही ऊखल का काम लेते हैं - दूसरे किसी साधनद्वारा फोड़ी हुई वस्तु नहीं ग्रहण करते। कोई पत्थरसे कूटकर खाते हैं, कोई जौ के आटे को पानी में उबालकर उसी को शुक्ल पक्ष या कृष्ण पक्ष में एक बार पी लेते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं, जो समय पर अपने-आप प्राप्त हुई वस्तु को ही भक्षण करते हैं। कोई मूल, कोई फल और कोई फूल खाकर ही नियमित जीवन व्यतीत करते हैं। इस प्रकार वे वानप्रस्थ के नियमों का दृढ़ता पूर्वक पालन करते हैं। वे मनीषी पुरुष ऊपर बताये हुए नाना प्रकार के नियमों की दीक्षा लेते हैं।
संन्यास आश्रम व्यवस्था
यह उपनिषदों द्वारा प्रतिपादित धर्म है। गृहस्थ और वानप्रस्थ प्रायः मिलते-जुलते माने गए हैं; किन्तु सन्यास इनसे भिन्न और विलक्षण है। इसमें अनेक प्रकार के उत्तम गुणों का निवास है। सर्वस्व-त्यागरूप संन्यास सबसे उत्तम आश्रम है। संन्यासी को चाहिये कि वह मोक्ष की सिद्धि के लिये अकेले ही धर्म का अनुष्ठान करे, किसी को साथ न रखे। जो ज्ञानवान् पुरुष अकेला विचरता है, वह सबका त्याग कर देता है; उसे स्वयं कोई हानि नहीं उठानी पड़ती। संन्यासी अग्निहोत्र के लिये अग्नि का चयन न करे, अपने रहने के लिये कोई घर न बनाये, केवल भिक्षा लेने के लिये ही गाँव में प्रवेश करे, कल के लिये किसी वस्तु का संग्रह न करे, मौन होकर शुद्धभाव से रहे तथा थोड़ा और नियमित भोजन करे। प्रतिदिन एक ही बार भोजन करे। भोजन करने और पानी पीने के लिये कपाल (काठ या नारियल आदिका पात्रविशेष) रखना, वृक्षकी जड़में निवास करना, मलिन वस्त्र धारण करना, अकेले रहना तथा सब प्राणियों की ओर से उदासीनता रखना — ये भिक्षु (संन्यासी)-के लक्षण हैं। जिस पुरुष के भीतर सबकी बातें समा जाती हैं — जो सबकी सह लेता है तथा जिसके पास से कोई बात लौटकर पुनः वक्ता के पास नहीं जाती — जो कटु वचन कहने वाले को भी कटु उत्तर नहीं देता, वही संन्यासाश्रम में रहने का अधिकारी है। कभी किसी की भी निन्दा को न तो करे और न सुने ही। विशेषतः ब्राह्मणों की निन्दा तो किसी तरह न करे। ब्राह्मण का जो शुभकर्म हो, उसी की सदा चर्चा करनी चाहिये। जो उसके लिये निन्दा की बात हो, उसके विषय में मौन रहना चाहिये। यही आत्मशुद्धि की दवा है।
जो जिस किसी भी वस्तुसे अपना शरीर ढक लेता है, जो कुछ मिल जाय उसी को खाकर भूख मिटा लेता है तथा जहाँ कहीं भी सो रहता है, उसे देवता ब्राह्मण (ब्रह्मवेत्ता) समझते हैं। जो जन-समुदाय को साँप समझकर, स्नेह-सम्बन्ध को नरक जानकर तथा स्त्रियों को मुर्दा समझकर उन सबसे डरता रहता है; उसे देवतालोग ब्राह्मण कहते हैं। जो मान या अपमान होनेपर स्वयं हर्ष अथवा क्रोधके वशीभूत नहीं होता, उसे देवतालोग ब्राह्मण मानते हैं। जो जीवन और मरण का अभिनन्दन न करके सदा काल की ही प्रतीक्षा करता रहता है, उसे देवता ब्राह्मण मानते हैं। जिसका चित्त राग-द्वेषादि के वशीभूत नहीं होता, जो इन्द्रियों को वश में रखता है तथा जिसकी बुद्धि भी दूषित नहीं होती, वह मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। जो सम्पूर्ण प्राणियों से निर्भय है तथा समस्त प्राणी जिससे भय नहीं मानते, उस देहाभिमान से मुक्त पुरुष को कहीं भी भय नहीं होता। जैसे हाथी के पदचिह्न में अन्य समस्त पादचारी जीवों के पदचिह्न समा जाते हैं तथा जिस प्रकार सम्पूर्ण ज्ञान चित्त में लीन हो जाते हैं, उसी प्रकार सारे धर्म और अर्थ अहिंसा में लीन रहते हैं।
इस प्रकार जो सबके प्रति समान भाव रखता है, भलीभाँति धैर्य धारण किये रहता है, इन्द्रियों को अपने वश में रखता है तथा सम्पूर्ण भूतों को त्राण देता है, वही ज्ञानी पुरुष उत्तम गति को प्राप्त होता है। जिसका अन्तः करण उत्तम ज्ञान से परितृप्त है तथा जिसमें ममता का सर्वथा अभाव है, उस मनीषी पुरुष की मृत्यु नहीं होती; वह अमृतत्व को प्राप्त हो जाता है। ज्ञानी मुनि सब प्रकार की आसक्तियों से मुक्त होकर आकाश की भाँति स्थित होता है। जो सबमें विष्णु की भावना करने वाला और शान्त होता है, उसे ही देवतालोग ब्राह्मण मानते हैं। जिसका जीवन धर्म के लिये, धर्म आत्मसन्तोष के लिये तथा दिन-रात पुण्य के लिये हैं, उसे देवता लोग ब्राह्मण समझते हैं। जिसके मन में कोई कामना नहीं होती, जो कर्मों के आरम्भ का कोई संकल्प नहीं करता तथा नमस्कार और स्तुति से दूर रहता है, जिसने योग के द्वारा कर्मों को क्षीण कर दिया है, उसे देवता लोग ब्राह्मण मानते हैं। सम्पूर्ण प्राणियों को अभय की दक्षिणा देना संसार में समस्त दानों से बढ़कर है। जो किसी की निन्दा का पात्र नहीं है तथा जो स्वयं भी दूसरों की निन्दा नहीं करता, वही ब्राह्मण परमात्मा का साक्षात्कार कर पाता है। जिसके समस्त पाप नष्ट हो गये हैं, जो इहलोक और परलोक में भी किसी वस्तु को पाने की इच्छा नहीं करता, जिसका मोह दूर हो गया है, जो मिट्टीके ढेले और सुवर्णको समान दृष्टि से देखता है, जिसने रोष को त्याग दिया है, जो निन्दा-स्तुति और प्रिय-अप्रिय से रहित होकर सदा उदासीन की भाँति विचरता रहता है, वही वास्तव में संन्यासी है।
- 168 min read
- 0
- 0